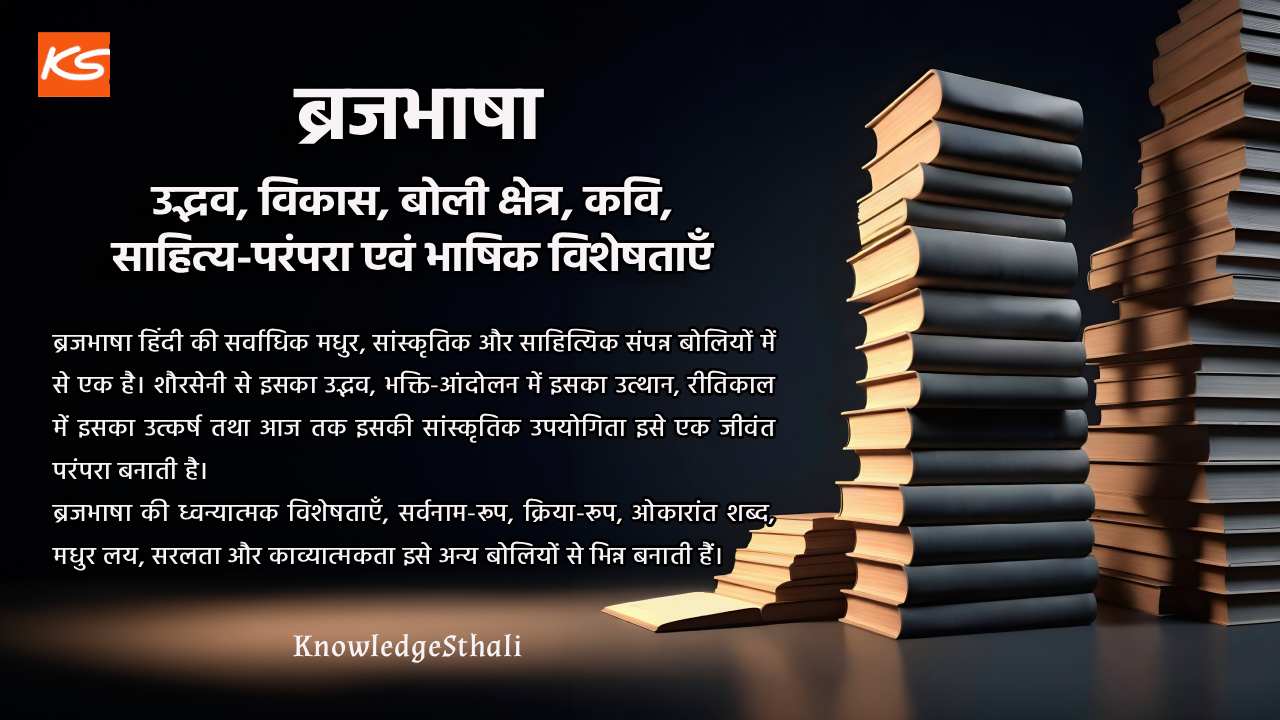भारतीय भाषाओं का इतिहास अत्यन्त प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। हिंदी भाषा के विकास में अनेक बोलियों ने अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं बोलियों में ब्रजभाषा एक अत्यंत प्रमुख और प्रतिष्ठित बोली है, जिसने न केवल हिंदी साहित्य के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, बल्कि भारतीय संस्कृति, भक्ति-आंदोलन, लोकजीवन और काव्यधारा को भी अनुपम रूप से समृद्ध किया है। ब्रजभाषा का क्षेत्र, परंपरा, काव्य और शैली आज भी हिंदी भाषाभाषियों और शोधार्थियों के लिए आकर्षण का विषय है।
ब्रजभाषा को हिंदी की पश्चिमी हिंदी शाखा की सर्वाधिक मधुर, सरस, काव्यात्म और ऐतिहासिक बोली माना जाता है। इसकी मधुरता, बोलचाल की सहजता, भावाभिव्यक्ति की क्षमता और रसप्रधान रचनाओं ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान दिलाया। सूर, नंददास, बिहारी, रत्नाकर, सेनापति से लेकर आधुनिक काल के कवियों तक ब्रजभाषा की परंपरा निरंतर चलती रही है।
यह लेख ब्रजभाषा की उत्पत्ति, विकास, भौगोलिक क्षेत्र, साहित्यिक परंपरा, भाषिक विशेषताएँ और हिंदी साहित्य में इसके योगदान पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है।
ब्रजभाषा का उद्भव और ऐतिहासिक विकास
ब्रजभाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी वह अपभ्रंश-भाषा थी जो मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ भागों में बोली जाती थी। कालांतर में इसी भाषा से पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ, जिनमें ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रमुख रही।
8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान शौरसेनी अपभ्रंश में अनेक साहित्यिक रचनाएँ हुईं। समय बीतने के साथ यह भाषा लोक-व्यवहार और साहित्य दोनों में परिवर्तित होती गई। यही भाषा 12वीं-13वीं शताब्दी तक ब्रजभाषा का रूप ग्रहण कर चुकी थी।
14वीं–17वीं शताब्दी ब्रजभाषा के स्वर्णकाल के रूप में जानी जाती है। इसी काल में
- सूरदास,
- नंददास,
- कृष्णदास,
- बिहारी,
- हितहरिवंश,
- देव,
- मतिराम,
- केशवदास
जैसे महान कवियों ने ब्रजभाषा को काव्य की ऊँचाइयों पर पहुँचाया।
संत-भक्ति आंदोलन के उत्तरकाल में ब्रजभाषा ने पूरे उत्तर भारत के साहित्यिक आकाश पर प्रभुत्व बनाया। आधुनिक काल से पूर्व तक हिंदी की मानक साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा ही मानी जाती थी।
ब्रजभाषा का भौगोलिक विस्तार
ब्रजभाषा मुख्यत: ब्रज मंडल की भाषा मानी जाती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
ब्रजभाषा के प्रमुख बोलने वाले क्षेत्र
ब्रजभाषा निम्नलिखित जिलों और क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है—
- मथुरा
- वृन्दावन
- आगरा
- भरतपुर
- धौलपुर
- करौली
- पश्चिमी ग्वालियर क्षेत्र
- अलीगढ़
- मैनपुरी
- बदायूँ
- बरेली
इन सभी क्षेत्रों का सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण ब्रजभाषा की मिठास से ओतप्रोत है। स्थानीय जनजीवन, लोकगीत, रीति-रिवाज, त्योहार, धार्मिक आयोजन सभी के माध्यम से ब्रजभाषा की पहचान आज भी सुरक्षित है।
ब्रज संस्कृति का प्रभाव
ब्रजभाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। कृष्ण-लीला, राधा-कृष्ण की उपासना, रस-परंपरा, होली के गीत, रास-लीला, मुरली-वादन, साहित्यिक रीतियाँ, ब्रज के लोक-नृत्य—ये सभी ब्रजभाषा के मूल तत्व हैं, जो इस क्षेत्र को विशिष्ट बनाते हैं।
ब्रजभाषा का साहित्यिक इतिहास और काव्य परंपरा
ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की सबसे समृद्ध और दीर्घकालिक साहित्यिक परंपराओं में से एक है।
संत-भक्ति काव्य में ब्रजभाषा
संत सूरदास और नंददास ने ब्रजभाषा को कृष्ण-भक्ति का श्रेष्ठ माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में—
- वात्सल्य भाव,
- माधुर्य भाव,
- सख्य भाव,
- दास्य भाव
जैसी भावनाएँ अत्यंत सहज और मधुरता से व्यक्त हुई हैं।
रीतिकालीन काव्य
रीतिकाल का अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में ही रचा गया। इस काल में ब्रजभाषा ने काव्य-सौंदर्य, अलंकारिता, रस-प्रधानता और वर्णन-कौशल का अद्वितीय प्रदर्शन किया।
इस काल के प्रमुख कवि—
- बिहारी (बिहारी सतसई)
- केशवदास
- देव
- पद्माकर
- गंगाधर
- चतुर्भुज दास
इन कवियों ने ब्रजभाषा को एक परिष्कृत, सुसंस्कृत और सौंदर्यप्रिय साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया।
ब्रजभाषा के प्रमुख कवि
ब्रजभाषा के कवियों की सूची अत्यंत विस्तृत है, परंतु निम्नलिखित प्रमुख कवियों को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है—
- सूरदास – ‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’
- नंददास – ‘सुरत-शतक’, ‘आनन्द-वृद्धि’
- बिहारी – ‘बिहारी-सतसई’
- धनानंद – ‘रसिक-प्रिया’
- सेनापति – ‘छंद-माला’
- देव – ‘देव-रसायन’, ‘काव्य-निर्णय’
- रसराज रत्नाकर
- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (आंशिक रूप से)
इन सभी कवियों ने ब्रजभाषा को काव्य-भाषा के रूप में सुदृढ़ आधार दिया।
ब्रजभाषा की भाषिक विशेषताएँ
ब्रजभाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि-व्यवस्था, शब्द-रूप और व्याकरण है। इसकी भाषा-संरचना खड़ी बोली और अन्य पश्चिमी हिंदी बोलियों से कुछ भिन्न है।
ओकारान्त शब्दों की प्रधानता
ब्रजभाषा में ओकारान्त शब्द अधिक प्रचलित हैं।
उदाहरण—
- छोटा → छोटो
- आया → आयो
- जाऊँगा → जाऊँगो
- दूजा → दूजो
खड़ी बोली के ‘ए’ और ‘ओ’ का ब्रज में ‘ऐ’ और ‘औ’ होना
उदाहरण—
- बेटा → बैटो
- बोला → बौलो
‘श’, ‘ष’, ‘स’ में ‘स’ की प्रधानता
ब्रजभाषा में ‘स’ का अधिक प्रयोग होता है।
उदाहरण—
- शिक्षक → सिक्खक
- राष्ट्र → रास्ट्र
‘ण’ ध्वनि का ‘न’ होना
मानक हिंदी का ‘ण’ ब्रजभाषा में ‘न’ हो जाता है।
उदाहरण—
- गणेश → गनेस
‘ड’, ‘ढ’, ‘ल’ का ‘र’ में परिवर्तन
उदाहरण—
- थोड़ा → थोरो
- बिजली → बिजुरी
सर्वनाम-प्रयोग की विशेषताएँ
उत्तम पुरुष
- मैं हौं
- मो, मोहि, मेरो
- हम, हमन, हमारौ
मध्यम पुरुष
- तू, तै, तो, तोहि
- तेरौ, तिहारौ
अन्य पुरुष
- वौ, वा, वे, वै
- इन, इन्हें, माहि
संबंधवाचक सर्वनाम
- जो, जे, जौ, जौन, जाहि
प्रश्नवाचक सर्वनाम
- कौ, कौन, का, काहि
अनिश्चयवाचक सर्वनाम
- कोई, कोऊ, काहू
बहुवचन में ‘अन’, ‘अनि’ का प्रयोग
उदाहरण—
- छोरौ → छोरनि
- लड़का → लरकानि
क्रियाओं में विशेष परिवर्तन
मानक हिंदी के नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत हो जाते हैं।
उदाहरण—
- चलना → चलनो
- दौड़ना → दौड़नो
ये सभी विशेषताएँ ब्रजभाषा को अन्य हिंदी बोलियों से अलग पहचान देती हैं।
ब्रजभाषा और लोकजीवन
ब्रजभाषा केवल साहित्यिक परंपरा तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोकगीतों, लोकनाट्य, रास-लीला, फाग गीत, कजरी, होली-गीत, मौर-गीत आदि में भी इसका व्यापक प्रयोग होता रहा है।
होली पर ब्रज के फाग, कृष्णलीला के पद, वृन्दावन के भजनों की मधुरता और रसभाव ब्रजभाषा के बिना संभव नहीं।
आधुनिक युग में ब्रजभाषा की स्थिति
आधुनिक काल में यद्यपि खड़ी बोली मानक हिंदी बन गई है, फिर भी ब्रजभाषा का सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक महत्व आज भी अविकसित नहीं हुआ।
- वृन्दावन और मथुरा की धार्मिक कथाओं में
- रास-लीला में
- भक्ति गीतों में
- सिनेमा और टीवी के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में
- लोकसाहित्य में
- सांस्कृतिक आयोजनों में
ब्रजभाषा की मधुरता और आकर्षण बरकरार है।
ब्रजभाषा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व
ब्रजभाषा का गहरा संबंध राधा-कृष्ण की लीलाओं से है।
कृष्ण और राधा की महिमा,
गोप-गोपियों की रासलीला,
यमुना तट की कथाएँ,
वृन्दावन की वन-लीला—
इन सभी का वर्णन ब्रजभाषा में ही सर्वाधिक भावपूर्ण ढंग से होता है। इसीलिए कृष्ण-भक्ति काव्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में ही संभव हो सकी।
ब्रजभाषा के 30 उदाहरण वाक्य
1–10 : सामान्य बोलचाल के वाक्य
- मैं हौं, तँ कहाँ जातो?
- तू मोहि काई न कह्यो?
- वौ लरको कित्ता सुंदर लागतो है।
- मोको पानी भिजाइ देओ।
- हमारौ घर यतै है।
- तुम्हारौ नाम कौ है?
- तू इतौ आओ, बात सुनौ।
- वई छोरी आज बजार गई थी।
- मोहि कछू भी न कह्यो।
- हम सब मिलि कै चलैं।
11–20 : क्रिया-प्रयोग और व्याकरणिक विशेषताओं वाले वाक्य
- मोहे चलनो है, देर न करौ।
- वौ कह्यो कि वहौ आवैगौ।
- तू खाना खायो कि नै?
- हमारौ काम काहे रुक गयो?
- तू जामनौ है कि यहीं रहनौ है?
- वौ तोहिकै देखि कै मुसकान दियो।
- तू मोहि किताब दै दै।
- हमहिं यहु काम करनौ है।
- इनै सब बातन की का जरूरत थी?
- तू काहे इतनो दुखी लागतो है?
21–30 : भक्ति, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वाक्य
- श्यामसुंदर घनश्याम गोकुल में खेलनौ आवै है।
- राधा रानी कौ रूप बहुत निरालौ है।
- सूरदास कहैं—“मो सो कछु न कहै।”
- ब्रज की धूली नै सब पाप हर लै है।
- कान्हा माखन खातौ फिरतौ है।
- गोपियन कहैं—“श्याम, मोहि छोड़ि कै कहाँ जातौ?”
- यमुना-तट पर रास रचाइ गई।
- ब्रज के वृक्षनि में बहुत हरियाली है।
- होरी खेलैं रसिया, ब्रज में रंग बरसै।
- वृन्दावन में श्रीकृष्ण की लीलनि सुनि कै मन हरषाय जातौ है।
निष्कर्ष
ब्रजभाषा हिंदी की सर्वाधिक मधुर, सांस्कृतिक और साहित्यिक संपन्न बोलियों में से एक है। शौरसेनी से इसका उद्भव, भक्ति-आंदोलन में इसका उत्थान, रीतिकाल में इसका उत्कर्ष तथा आज तक इसकी सांस्कृतिक उपयोगिता इसे एक जीवंत परंपरा बनाती है।
ब्रजभाषा की ध्वन्यात्मक विशेषताएँ, सर्वनाम-रूप, क्रिया-रूप, ओकारांत शब्द, मधुर लय, सरलता और काव्यात्मकता इसे अन्य बोलियों से भिन्न बनाती हैं।
आज भी जब कोई व्यक्ति ब्रजभाषा के पद या भजन सुनता है, तो मन में सहज ही रस, प्रेम, माधुर्य और भक्तिभाव उमड़ पड़ता है। यही ब्रजभाषा का सौंदर्य और जीवन्तता है।
इन्हें भी देखें –
- हिन्दी की बोलियाँ : विकास, स्वरूप, उपभाषा, वर्गीकरण और साहित्यिक योगदान
- मैथिली भाषा : इतिहास, विकास, लिपि और साहित्यिक महत्त्व
- नेपाली भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, दिवस और साहित्य
- भोजपुरी भाषा : इतिहास, विकास, लिपि, क्षेत्र, साहित्य और विशेषताएँ
- भारत की शास्त्रीय भाषाएँ : भाषाई विरासत, मानदंड, विकास और महत्व
- राष्ट्रभाषा हिन्दी – निबंध : राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का प्रबल आधार
- बूढ़ी काकी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व
- हिंदी वर्णमाला में व्यंजन : परिभाषा, प्रकार और भेद
- राज्यों का बढ़ता सार्वजनिक ऋण : एक गंभीर चुनौती
- पाक–सऊदी रक्षा समझौता: पश्चिम एशिया की बदलती भू–राजनीति
- भारतीय संसद | लोक सभा और राज्य सभा | राज्यों में सीटें
- भारत में महारत्न कंपनियों की सूची