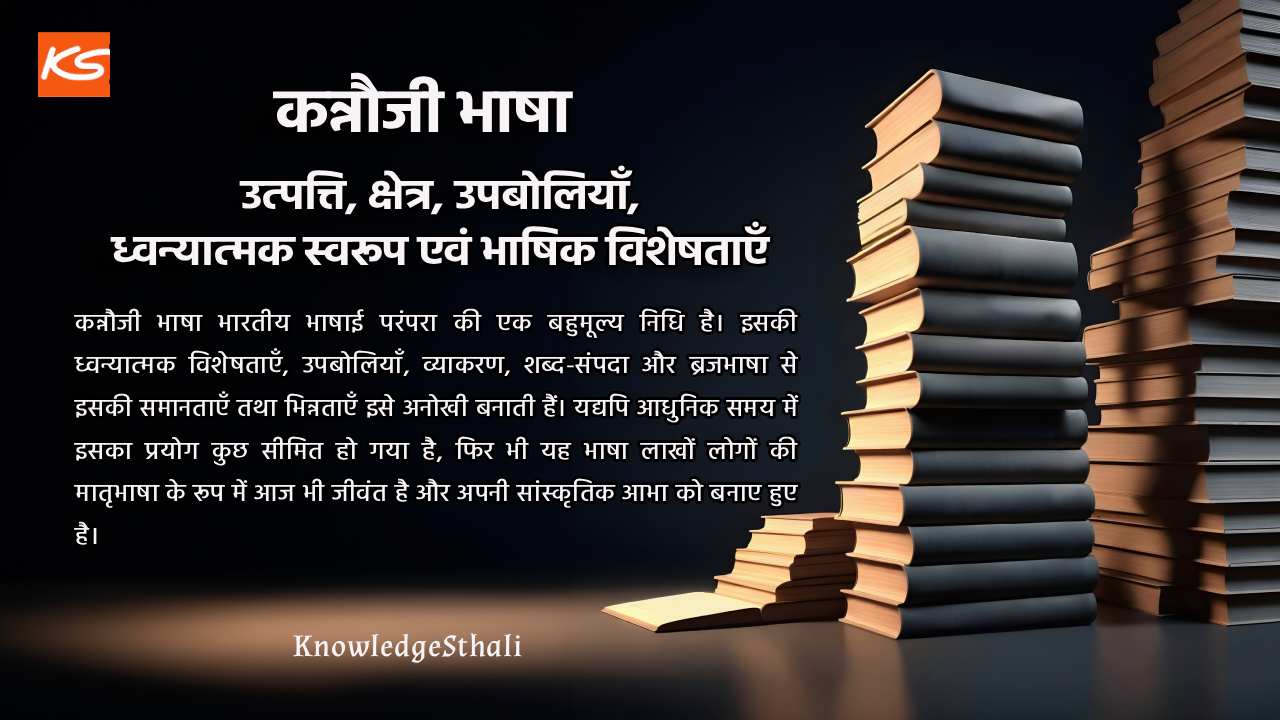भारतीय उपमहाद्वीप भाषाई विविधता के अप्रतिम समृद्ध भंडार का प्रतीक है। यहाँ “कोस-कोस पर पानी बदले, दुइ-दुइ कोस पर बानी”—यह कहावत केवल कहावत नहीं, बल्कि भाषा-विज्ञान का जीवंत सत्य है। इसी भाषाई-विविधता में एक महत्वपूर्ण स्थान कन्नौजी भाषा (या कन्नौजिया/कनउजी) का है, जो पश्चिमी हिन्दी का एक प्रमुख रूप है। कन्नौज भारतीय इतिहास, संस्कृति, राजनीति और भाषिक परंपरा का अत्यंत प्राचीन और महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा है। कन्नौज की भाषा—कन्नौजी—अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक बनावट, उपबोलियों, व्याकरण, उच्चारण शैली तथा ऐतिहासिक विकास के कारण हिन्दी भाषाई परिवार में एक अलग पहचान रखती है।
यह लेख कन्नौजी भाषा के इतिहास, उत्पत्ति, भौगोलिक विस्तार, उपबोलियों, ध्वन्यात्मक संरचना, व्याकरणिक स्वरूप और ब्रजभाषा से इसके अंतर को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करता है।
कन्नौज : ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
कन्नौज, उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण जिला, ऐतिहासिक रूप से “कन्याकुब्ज” के नाम से जाना जाता रहा है। यह नगर भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रतीत होता है, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, पुराणों, बौद्ध साहित्य तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। मध्यकाल में कन्नौज भारत की राजनीति का केंद्र रहा और तीन राजाओं—यशोवर्मा, हर्षवर्धन तथा बाद में गुर्जर प्रतिहारों—के कारण यह “कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष” का केंद्र बना।
इतिहास जितना समृद्ध, भाषा भी उतनी ही गहन और सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण है।
कन्नौजी भाषा की उत्पत्ति
भाषावैज्ञानिक दृष्टि से कन्नौजी का विकास शौरसेनी प्राकृत की उपशाखा पांचाली प्राकृत से हुआ है।
- आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कन्नौजी को “पांचाली” नाम दिया है।
- पांचाल प्रदेश (वर्तमान: कन्नौज, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद आदि) की मुख्य बोली होने के कारण इसे यह नाम मिला।
- शौरसेनी से विकसित अधिकांश बोलियों का स्वरूप आधुनिक पश्चिमी हिंदी में मिलता है, अतः कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी परिवार का अंग है।
इस तरह कहा जा सकता है कि कन्नौजी भारतीय आर्यभाषाओं की हजारों वर्षों की विकास-यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।
कन्नौजी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र
कन्नौजी बोली भले ही देश की प्रमुख भाषाओं में से न हो, परंतु इसका क्षेत्रीय महत्व बहुत अधिक है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में पाई जाती है—
कन्नौजी बोली के मुख्य क्षेत्र
- कन्नौज
- औरैया
- कानपुर देहात एवं कनपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र
- इटावा
- मैनपुरी
- फर्रुखाबाद
- शाहजहाँपुर
- हरदोई
- पीलीभीत
इन क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में कन्नौजी का प्रयोग अत्यंत व्यापक है।
पश्चिम में ब्रजभाषा का प्रभाव
कन्नौज की पश्चिमी सीमा पर ब्रजभाषा बोली जाती है। यही कारण है कि दोनों भाषाओं का उच्चारण, शब्दावली और संरचना अनेक स्थानों पर एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। अक्सर भाषाविद् दोनों को पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं, हालांकि कन्नौजी में कुछ विशिष्ट ध्वन्यात्मक संरचनाएँ हैं, जो इसे ब्रज से अलग करती हैं।
कन्नौजी की उपबोलियाँ
भाषिक व्यवहार में कन्नौजी का विस्तार सीमित होते हुए भी इसकी उपबोलियाँ आश्चर्यजनक रूप से विविध हैं। यह विविधता भारतीय भाषाओं की प्रकृति से मेल खाती है, क्योंकि ग्राम-विन्यास के अनुसार भाषा के स्वरूप में बदलाव स्वतः उत्पन्न होते हैं।
मुख्य उपबोलियाँ
- मध्य कन्नौजी
- तिरहारी
- पछरुआ
- बंग्रही
- शाहजहाँपुरिया
- पीलीभीती
- बदउआँ
- अन्तर्वेदी
इन उपबोलियों में शब्द, उच्चारण, ध्वनि-रूप, लय और व्याकरण में सूक्ष्म अंतर दिखाई देते हैं।
ओकारान्त प्रवृत्ति : पहचान का आधार
कन्नौजी बोली की सबसे मुख्य पहचान इसका ओकारान्त स्वरूप है, अर्थात्—
कन्नौजी में शब्दों, विशेषकर क्रियाओं के अंत में ‘ओ’ का अधिक प्रयोग होता है।
उदाहरण:
- गयो → गयो/गओ
- खायो → खायौ
- करयो → करै
- चलयो → चलै
यह संरचना कन्नौजी को ब्रज और अन्य पश्चिमी हिंदी बोलियों से अलग करती है।
ब्रजभाषा और कन्नौजी का तुलनात्मक अध्ययन
ब्रजभाषा और कन्नौजी दोनों पश्चिमी हिन्दी परिवार की बोलियाँ हैं और कई मामलों में एक-दूसरे से मिलती-जुलती भी हैं। किंतु कुछ मूलभूत अंतर इन्हें स्वतंत्र भाषाई पहचान प्रदान करते हैं।
(क) ध्वनि-रूप में अंतर
1. ब्रज की ऐ तथा औ → कन्नौजी में अइ और अउ
- कौन → कउन
- बैल → बइल
- और → अउर
2. कन्नौजी में ओ और ए का प्रयोग जबकि ब्रज में ऐ और औ
उदाहरण के लिए—
- ब्रज में: खायौ
- कन्नौजी में: खायो / खायौ
3. स्वर-संरचना में संयुक्त स्वरों की प्रबलता
कन्नौजी में अइ, अउ, अऊ जैसे संयुक्त स्वर सामान्य हैं।
कन्नौजी बोली की ध्वन्यात्मक विशेषताएँ
कन्नौजी बोली की ध्वनियाँ इसके भाषिक व्यक्तित्व की मूल आधारशिला हैं। इन ध्वनियों में अनेक विशिष्टताएँ हैं—
(1) ‘ह’ का लोप
मध्य ‘ह’ अक्सर लुप्त हो जाता है—
- जाहि
- जाइ
- कहो → कओ
(2) शब्दारम्भ में विशेष व्यंजन-समूह
कन्नौजी में शब्दारम्भ में ल्ह, र्ह, म्ह जैसे संयोजन मिलते हैं—
- ल्हसुन
- र्हँट (रेंगन/बैंगन का पौधा)
- म्हँगाई
यह संरचना हिंदी की अन्य बोलियों में दुर्लभ है।
(3) अन्त्य ध्वनि में अल्पप्राण से महाप्राण रूपांतरण
- हाथ → हात्
- दांत → दात्
(4) अनुनासिकीकरण की विशेष प्रवृत्ति
कन्नौजी में स्वरों का नासिकीकरण बहुत अधिक है—
- अइँचत
- जुआँ
- मों (मुँह)
- उंघियात
- भउजाई
- अनेंठ
(5) ‘य’ → ‘ज’
- यमुना → जमुना
- यश → जस
(6) ‘व’ → ‘ब’
- वकील → बकील
- वर → बर
कुछ स्थानों पर व → उ भी हो जाता है—
- अवतार → अउतार
(7) अवधी की भाँति उकारान्त शब्द
- खेत → खेतु
- मरत → मत्तु
(8) ‘ख’ → ‘क’
- भीख → भीक
- खून → कून
(9) ‘ण’ → ‘ड़’
- गण → गड़
- रावण → रावड़
(10) ‘स’ → ‘ह’
कई संज्ञाओं में स के स्थान पर ह हो जाता है—
- सप्ताह → हप्ताह
- मास्टर → महट्टर
(11) उपेक्षा-सूचक “टा” प्रत्यय
कई संज्ञाओं के साथ टा लगाकर उन्हें हल्के-फुल्के, उपेक्षापूर्ण या हास्यात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है—
- बच्चा → बच्चटा
- किसान → किसन्टा
- बनिया → बनेटा
- काछी → कछेटा
यह प्रत्यय कन्नौजी की एक अत्यंत रोचक और विशिष्ट विशेषता है।
कन्नौजी भाषा का व्याकरण
कन्नौजी भाषा का व्याकरण सरल होते हुए भी विशिष्ट है। इसमें हिंदी और ब्रजभाषा के अनेक तत्व शामिल हो जाते हैं, किंतु कन्नौजी का स्वतन्त्र स्वरूप उसकी क्रिया-योजना, कारक-विभक्ति और वाक्य-रचना में स्पष्ट दिखाई देता है।
(1) संज्ञा और लिंग
कन्नौजी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप सामान्यतः हिंदी जैसे हैं, परंतु उच्चारण में परिवर्तन दिखाई देता है—
- लड़का → लरको
- लड़की → लरकीया
(2) कारक-रूप
कारक चिह्न अक्सर अपभ्रंश रूपों में प्रकट होते हैं—
- राम के घर → रामै घर
- मोहन को → मोहनौ
- उसको → ओकै
(3) सर्वनाम
कन्नौजी के सर्वनाम हिंदी से भिन्न ध्वन्यात्मक रूप में मिलते हैं—
- मैं → हम
- तुम → तू/तुमै
- वह → उ/ऊ
- ये/वे → एहैं/ओहैं
(4) क्रिया-रूप
कन्नौजी की क्रियाएँ ओकारान्त रूपों में समाप्त होती हैं—
वर्तमान काल
- मैं जाता हूँ → हम जायित हौं
- वह खाता है → उ खायतो
भूतकाल
- वह गया → उ गओ / गयो
- मैंने खाया → हम खायो
भविष्यत् काल
- वह जाएगा → उ जाइबो
- तुम करोगे → तुम करइबो
(5) नकारात्मक वाक्य
नकार सूचक शब्द—
- नइ
- नाइ
- नहुं
उदाहरण—
- मैं नहीं जाऊँगा → हम नइ जाइबो
(6) वाक्य संरचना
सामान्यतः SOV क्रम—
- उ दुकान गओ।
- मोहनौ दूध लइआओ।
कन्नौजी की शब्द-संपदा
कन्नौजी शब्दावली अत्यंत समृद्ध है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, खड़ी बोली तथा अवधी के तत्व सम्मिलित हैं।
कुछ विशिष्ट शब्द—
- कउन (कौन)
- कछु (कुछ)
- गोंई (गाय)
- तौ (तो)
- आयौ (आया)
- जउन (जो)
- भइया (भाई)
कन्नौजी में ‘अउ’, ‘अइ’, ‘अऊ’ जैसे स्वर-समूह अनेक शब्दों में मिलते हैं, जो इसकी पहचान हैं।
साहित्य और कन्नौजी भाषा
कन्नौजी में विशिष्ट साहित्य कम लिखा गया है, क्योंकि यह मुख्यतः बोली आधारित भाषा है। किंतु लोकगीत, कहावतें, मुहावरे, पारंपरिक कथाएँ अत्यधिक समृद्ध हैं।
कन्नौजी के लोकगीतों में—
- सोहर
- कजरी
- फाग
- आल्हा
- बिरहा
का व्यापक उपयोग है।
लोकभाषा के गीत जीवन की अनुभूतियों, कृषि-प्रधान संस्कृति, परिवार, प्रकृति, प्रेम और त्यौहारों की भावनाओं से भरे होते हैं।
कन्नौजी : आधुनिक परिप्रेक्ष्य
आज के समय में कन्नौजी बोली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित है। शहरीकरण, शिक्षा, मीडिया और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण कन्नौजी की जगह धीरे-धीरे खड़ी बोली हिंदी ले रही है।
फिर भी—
- कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्रों में
- त्यौहारों और संस्कार-गीतों में
- पारिवारिक बातचीत में
- बुजुर्गों की बोली में
यह आज भी एक प्रबल जीवंत भाषा के रूप में कायम है।
कन्नौजी का भाषाई महत्व
कन्नौजी केवल एक बोली नहीं, बल्कि—
- सांस्कृतिक धरोहर
- ऐतिहासिक पहचान
- भाषाई विविधता का प्रतीक
- पश्चिमी हिंदी और प्राकृत परंपरा का सेतु
है।
भाषाविदों के लिए कन्नौजी अध्ययन की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है क्योंकि इसमें प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और आधुनिक हिंदी के बीच विकसित भाषा-परिवर्तन की अनेक अवस्थाएँ दिखाई देती हैं।
कन्नौजी भाषा के उदाहरण वाक्य
1. सामान्य बातचीत
- तू कहाँ जातो?
(तुम कहाँ जा रहे हो?) - हम घर जात हौं।
(मैं घर जा रहा हूँ।) - उ कउन है?
(वह कौन है?) - मोै तोहसे कहत हौं।
(मैं तुमसे कह रहा हूँ।)
2. परिवार और रिश्तों से जुड़े वाक्य
- भइया खेत मा गओ।
(भाई खेत में गया।) - अम्मा खाना बनावत अहैं।
(माँ खाना बना रही हैं।) - बच्चटा स्कूल गओ कि नइ?
(वह बच्चा स्कूल गया या नहीं?)
3. क्रिया-रूप वाले वाक्य
- हम खायो हौं।
(मैं खा चुका हूँ।) - उ पानी पियतो है।
(वह पानी पी रहा है।) - तू किताब लइआओ।
(तुम किताब ले आओ।) - उ गओ अउ फटाफट आवै।
(वह गया और तुरंत आएगा।)
4. नकारात्मक वाक्य
- हम नइ जाइबो।
(मैं नहीं जाऊँगा।) - तू क्यों नइ बोलतो?
(तुम क्यों नहीं बोलते?) - उ स्कूल नइ गओ।
(वह स्कूल नहीं गया।)
5. प्रश्नवाचक वाक्य
- एहै कउन किताब?
(यह कौन-सी किताब है?) - कइतौ बज गओ?
(कितना बज गया?) - तू का करत हौ?
(तुम क्या कर रहे हो?)
6. आदेश/अनुरोध वाले वाक्य
- तू पानी लइआओ।
(तुम पानी ले आओ।) - इहाँ बैठो।
(यहाँ बैठो।) - मोका सुनइ लओ।
(मेरी बात सुन लो।)
7. व्यवहारिक वाक्य
- हमार घर उहैं है।
(मेरा घर वहीं है।) - मोका भउख लागी है।
(मुझे भूख लगी है।) - उ बहुत तेज बोलतो है।
(वह बहुत तेज बोलता है।)
8. ग्रामीण/स्थानीय संदर्भ के वाक्य
- बइया बैलवा खेतु मा जोततो है।
(बड़ी मुश्किल से बैल खेत में जुत रहा है।) - बउरही मड़इया मा रहत हैं।
(बुज़ुर्ग झोपड़ी में रहते हैं।) - बरखा आवै का चान्ह लगत है।
(बारिश आने के संकेत लग रहे हैं।)
निष्कर्ष
कन्नौजी भाषा भारतीय भाषाई परंपरा की एक बहुमूल्य निधि है। इसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएँ, उपबोलियाँ, व्याकरण, शब्द-संपदा और ब्रजभाषा से इसकी समानताएँ तथा भिन्नताएँ इसे अनोखी बनाती हैं। यद्यपि आधुनिक समय में इसका प्रयोग कुछ सीमित हो गया है, फिर भी यह भाषा लाखों लोगों की मातृभाषा के रूप में आज भी जीवंत है और अपनी सांस्कृतिक आभा को बनाए हुए है।
कन्नौजी भाषा का अध्ययन भारत की भाषाई विविधता को समझने और भारतीय आर्यभाषा परिवार को गहराई से जानने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
इन्हें भी देखें –
- बुंदेली – बुंदेली बोली – बुंदेलखंडी भाषा – पश्चिमी हिन्दी : उत्पत्ति, क्षेत्र, विशेषताएँ और भाषिक वैभव
- भाषा : परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएँ, शैली और उत्पत्ति
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- हिंदी साहित्य का मध्यकाल : भक्ति और रीति धाराओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप
- भारत में मध्यकालीन साहित्य: फ़ारसी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में शैलियों का विकास
- रीतिकाल के कवि और रचनाएँ
- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार
- बोड़ो या बड़ो भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, बोली क्षेत्र और सांस्कृतिक महत्व
- संस्कृत भाषा : इतिहास, उत्पत्ति, विकास, व्याकरण, लिपि और महत्व