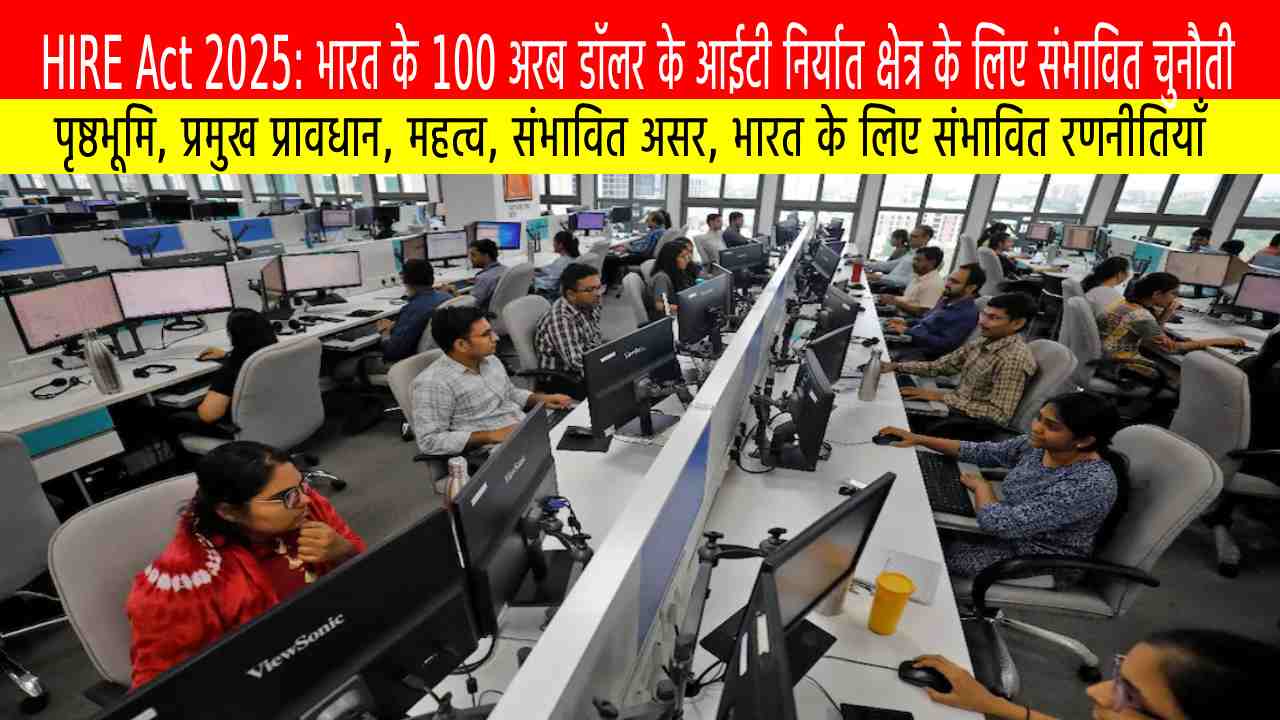भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक स्तंभ बन चुका है। वर्ष 2025 तक यह उद्योग 100 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारतीय आईटी कंपनियाँ—टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ और टेक महिंद्रा—विश्व की अग्रणी तकनीकी सेवा प्रदाताओं में गिनी जाती हैं और अमेरिकी बाज़ार इनकी आय का प्रमुख आधार है।
इसी बीच अमेरिका में प्रस्तुत किया गया एक नया विधेयक—HIRE Act 2025 (Halting International Relocation of Employment Act)—ने पूरे भारतीय आईटी उद्योग और नीति-निर्माताओं के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। यदि यह अधिनियम पारित हो जाता है तो भारत के लिए इसके गहरे आर्थिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ होंगे।
HIRE Act 2025 की पृष्ठभूमि
अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग से घरेलू रोजगार के अवसरों में कमी आती है। विशेषकर आईटी और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियाँ लागत कम करने के लिए भारत और फिलीपींस जैसे देशों पर निर्भर रही हैं।
ट्रम्प प्रशासन से लेकर बाइडेन प्रशासन तक “Buy American” और “Bring Jobs Back Home” जैसी नीतियाँ सामने आती रही हैं। इन्हीं नीतिगत प्रयासों की श्रृंखला में HIRE Act 2025 को देखा जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि अमेरिकी कंपनियाँ विदेशों में सेवाएँ आउटसोर्स करने के बजाय देश के भीतर अधिक रोजगार सृजन करें।
HIRE Act 2025 के प्रमुख प्रावधान
यह अधिनियम सिर्फ नीतिगत घोषणा भर नहीं है, बल्कि इसमें कई सख्त वित्तीय और कानूनी प्रावधान शामिल हैं:
- 25% उत्पाद शुल्क (Excise Tax):
अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं को दी जाने वाली फीस, रॉयल्टी, या सेवा शुल्क पर 25% कर लगाया जाएगा, यदि इन सेवाओं का लाभ अमेरिकी उपभोक्ताओं को मिलता है। - कर कटौती की अनुमति नहीं:
अब तक कंपनियाँ ऐसे खर्चों को अपने कर योग्य आय से घटा सकती थीं, लेकिन इस अधिनियम के तहत यह छूट समाप्त हो जाएगी। इससे वास्तविक लागत और भी बढ़ जाएगी। - अपॉर्शनमेंट क्लॉज़:
यदि कोई सेवा आंशिक रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं और आंशिक रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाती है, तो कर अनुपातिक आधार पर लगाया जाएगा। - बढ़ी हुई अनुपालन आवश्यकताएँ:
कंपनियों को विस्तृत रिपोर्टिंग करनी होगी, कॉर्पोरेट अधिकारियों से प्रमाणन लेना होगा और गलत जानकारी पर भारी दंड भुगतना होगा। - घरेलू कार्यबल कोष:
इस कर से प्राप्त धनराशि अमेरिकी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। - प्रभावी तिथि:
यदि अधिनियम पारित हो जाता है तो यह 31 दिसंबर 2025 के बाद किए गए सभी भुगतानों पर लागू होगा।
भारत के लिए HIRE Act 2025 का महत्व
अमेरिका भारतीय आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अनुमान है कि भारतीय आईटी निर्यात का लगभग 60% हिस्सा अकेले अमेरिकी बाज़ार से आता है। ऐसे में इस अधिनियम के निम्नलिखित असर हो सकते हैं:
- लागत में भारी वृद्धि:
यदि अमेरिकी कंपनी भारत को 100 डॉलर का भुगतान करती है, तो उसे लगभग 46 डॉलर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा (25 डॉलर उत्पाद शुल्क + 21 डॉलर कर कटौती का नुकसान)। - प्रतिस्पर्धा में कमी:
भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी कंपनियों और स्थानीय प्रदाताओं के मुकाबले अपनी लागत-प्रभावशीलता खो सकती हैं। - विस्तृत प्रभाव:
केवल बड़ी कंपनियाँ ही नहीं, बल्कि कैप्टिव सेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और यहाँ तक कि फ्रीलांसर तक प्रभावित होंगे।
संभावित असर (यदि अधिनियमित हुआ)
- मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता पर दबाव:
कंपनियों को नए अनुबंध करने होंगे या लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना होगा। - अनुपालन और अनुबंध पुनर्गठन:
कंपनियों को सेवाओं की भौगोलिक संरचना बदलनी पड़ सकती है और उपभोक्ता स्थान का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा। - ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) रणनीति में बदलाव:
अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों में नए GCCs स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। - स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी:
लागत घटाने के लिए कंपनियाँ एआई और रोबोटिक्स को अधिक अपनाएँगी। - व्यापारिक और नीति तनाव:
अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव आ सकता है यदि भारत इस अधिनियम से छूट (carve-out) नहीं प्राप्त कर पाया।
क्षेत्रवार असर
- आईटी सेवाएँ और एप्लीकेशन डेवलपमेंट:
सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अमेरिकी क्लाइंट्स इन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करते हैं। - बीपीएम और कॉल सेंटर्स:
सीधे प्रभावित, क्योंकि इनकी सेवाएँ स्पष्ट रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ देती हैं। - प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और आरएंडडी:
असर इस पर निर्भर करेगा कि अंतिम उत्पाद उपभोक्ता-उन्मुख है या बिज़नेस-टू-बिज़नेस। - फ्रीलांसर और स्टार्टअप्स:
छोटे अमेरिकी स्टार्टअप्स को भी वैश्विक फ्रीलांसर रखने पर अधिक लागत झेलनी होगी।
भारत के लिए संभावित रणनीतियाँ
- नीतिगत बातचीत:
भारत को अमेरिका से छूट (carve-out) की मांग करनी चाहिए, विशेषकर आईटी सेवाओं के लिए। - विविधीकरण:
भारतीय कंपनियों को यूरोप, एशिया-प्रशांत और अफ्रीका के नए बाज़ारों में विस्तार करना होगा। - स्वचालन और नवाचार:
लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड-आधारित समाधान अपनाने होंगे। - घरेलू बाज़ार पर ध्यान:
भारत में ही बढ़ते डिजिटलीकरण और सरकारी पहलों (जैसे डिजिटल इंडिया) का लाभ उठाया जा सकता है। - जीसीसी सहयोग:
भारतीय आईटी कंपनियाँ वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर हाइब्रिड मॉडल बना सकती हैं, जिसमें कुछ काम अमेरिका में और कुछ भारत में हो।
अंतरराष्ट्रीय और भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
HIRE Act 2025 केवल आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक भू-राजनीतिक संदेश भी है। अमेरिका अपने घरेलू कार्यबल की सुरक्षा करना चाहता है और चीन, भारत जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर निर्भरता घटाना चाहता है।
भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका के साथ अपने तकनीकी और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखते हुए अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी सुरक्षित रखे।
महत्वपूर्ण तथ्य (Revision Notes)
- विधेयक का नाम: HIRE Act 2025 (Halting International Relocation of Employment)
- मुख्य प्रावधान: 25% उत्पाद शुल्क + कर कटौती की हानि
- प्रभावी तिथि: 31 दिसंबर 2025 के बाद के भुगतान
- भारत के लिए असर: आईटी सेवाएँ, बीपीओ, फ्रीलांसर और जीसीसी पर प्रतिकूल प्रभाव
- संभावित समाधान: नीतिगत छूट, स्वचालन, बाज़ार विविधीकरण, घरेलू बाज़ार पर ध्यान
निष्कर्ष
HIRE Act 2025 भारत के आईटी निर्यात उद्योग के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह केवल लागत और अनुबंधों का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक तकनीकी स्थिति, रोजगार और विदेशी मुद्रा आय पर भी असर डाल सकता है।
हालाँकि, भारतीय आईटी उद्योग ने हमेशा संकटों को अवसर में बदला है—चाहे वह Y2K की चुनौती रही हो, 2008 की वैश्विक मंदी या कोविड-19 का संकट। ऐसे में यह उद्योग नए नवाचार, स्वचालन और बाज़ार विविधीकरण के माध्यम से इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है।
इन्हें भी देखें –
- मस्तिष्क खाने वाला अमीबा: (Naegleria fowleri): केरल में बढ़ता खतरा, लक्षण, बचाव
- जेनरेशन Z: नेपाल आंदोलन, विशेषताएँ, Millennials और Generation Alpha से तुलना
- ऑस्ट्रेलिया के “घोस्ट शार्क”: नौसैनिक युद्ध में आने वाला बड़ा परिवर्तन
- ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारतीय लिपियों तक: उद्भव, विकास, शास्त्रीय प्रमाण, अशोक शिलालेख
- लिपि : परिभाषा, अर्थ, इतिहास, प्रकार, रूपांतरण और उदाहरण
- दृश्य काव्य : परिभाषा, स्वरूप, भेद, उदाहरण और साहित्यिक महत्त्व