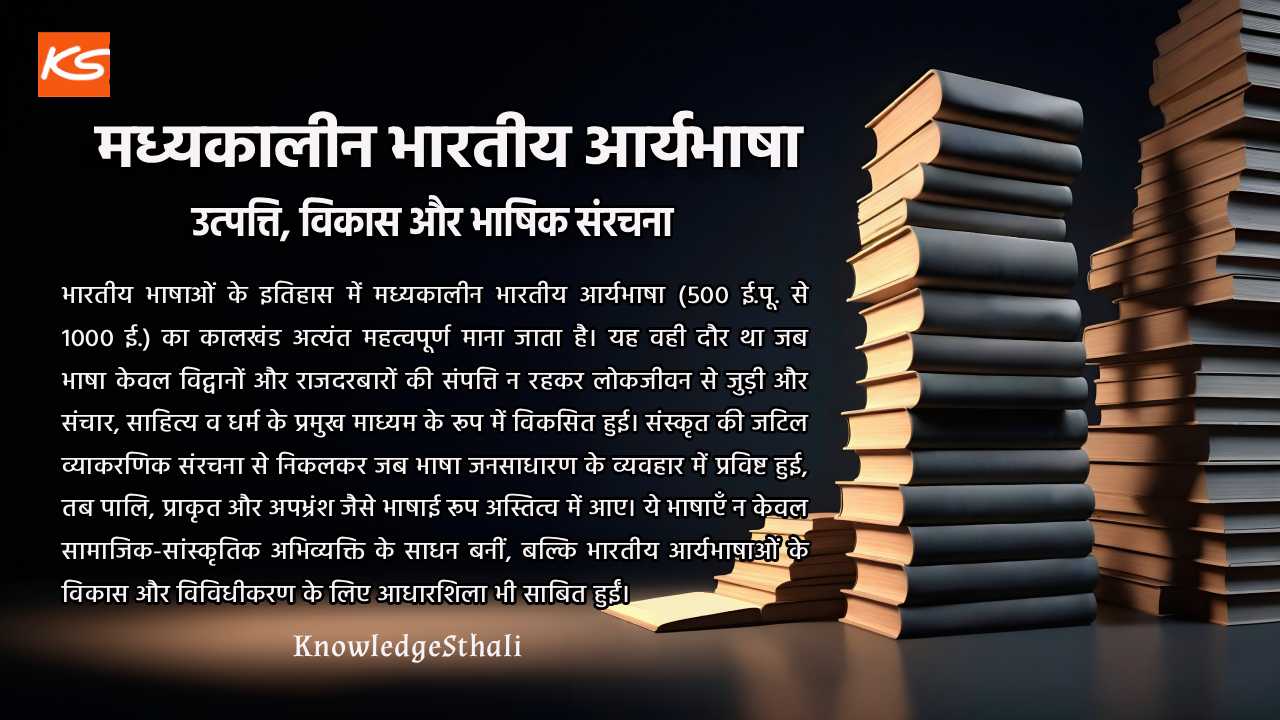भारतीय भाषाओं के इतिहास में मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का कालखंड अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वही दौर था जब भाषा केवल विद्वानों और राजदरबारों की संपत्ति न रहकर लोकजीवन से जुड़ी और संचार, साहित्य व धर्म के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित हुई। संस्कृत की जटिल व्याकरणिक संरचना से निकलकर जब भाषा जनसाधारण के व्यवहार में प्रविष्ट हुई, तब पालि, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे भाषाई रूप अस्तित्व में आए। ये भाषाएँ न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साधन बनीं, बल्कि भारतीय आर्यभाषाओं के विकास और विविधीकरण के लिए आधारशिला भी साबित हुईं।
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं ने एक ओर बौद्ध व जैन दर्शन की लोकपरक अभिव्यक्ति को संभव बनाया और दूसरी ओर साहित्यिक सृजन को सरलता, सहजता और मानवतावादी दृष्टि प्रदान की। इसी काल में भाषा ने पांडित्य से व्यावहारिकता और राजकीय सीमा से जनसांस्कृतिक विस्तार की ओर संक्रमण किया। आगे चलकर इन्हीं भाषिक रूपों से हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ विकसित हुईं।
अतः मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का अध्ययन केवल भाषिक इतिहास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति के विकास को समझने की दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है।
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा : परिचय
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ईस्वी) भारतीय भाषाओं के उस संक्रमणकाल को दर्शाती है जिसमें भाषा रूपांतरण, सरलीकरण और लोकजीवन से गहन संपर्क के चलते अपने आधुनिक स्वरूप की ओर अग्रसर हुई। यह काल लगभग 500 ई.पू. से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस अवधि में भाषा न केवल व्याकरणीय रूप से परिवर्तित हुई, बल्कि ध्वनि, शब्द, रूप-विधान और वाक्य-रचना में भी उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देते हैं।
इस चरण में साहित्य और धार्मिक ग्रंथों की रचना में संस्कृत के स्थान पर सरल भाषाएँ अपनाई जाने लगीं। पालि भाषा इस युग की शुरुआत में प्रचलित हुई, जिसने बौद्ध साहित्य तथा धम्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद प्राकृत भाषाएँ सामने आईं, जिनका उपयोग नाटक, कथाओं, चरित साहित्य और जैन धर्म के ग्रंथों में व्यापक रूप से हुआ। समय के साथ जब प्राकृत रूप और सरल, बोलचाल के अनुकूल होता गया, तो उससे अपभ्रंश भाषा विकसित हुई, जिसे आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का अंतिम मध्यकालीन स्वरूप माना जाता है।
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं के विकास में प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार दिखाई देते हैं—
- ध्वनियों की सहजता और सरलीकरण
- संस्कृत के तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों का प्रयोग
- विभक्तियों का लोप और परसर्गों का प्रयोग
- लिंग, वचन और क्रिया-रूपों का सरलकरण
इस काल में भाषा का स्वरूप जन-संचार के और अधिक निकट आता गया, और परिणामस्वरूप भाषा केवल अभिजात और विद्वानों की ही नहीं, बल्कि जनसाधारण की भी अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। आगे चलकर इसी चरण से हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी एवं बंगाली जैसी प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाएँ विकसित हुईं।
अतः मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ भारतीय भाषिक इतिहास की वह महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिन्होंने शास्त्रीय अभिव्यक्ति से लोकभाषा की ओर परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और आधुनिक भाषाओं की नींव तैयार की।
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का काल-विभाजन (500 ई.पू. – 1000 ई.)
भारतीय भाषाओं के विकास क्रम में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कालखंड में भाषा संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर आगे चलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं—जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि—का निर्माण हुआ। यह काल न केवल भाषायी संक्रमण का समय था, बल्कि भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के विकास का भी महत्वपूर्ण दौर रहा।
भाषावैज्ञानिक दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है—
इन तीनों चरणों में भाषा की संरचना धीरे-धीरे संस्कृत की जटिल व्याकरणिक प्रणाली से सरल, बोलचाल की अभिव्यक्ति की ओर विकसित होती गई। इस लेख में वर्तमान चरण में पालि (प्रथम प्राकृत) प्राकृत (द्वितीय प्राकृत) और अपभ्रंश (तृतीय प्राकृत) का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है —
1. पालि भाषा (500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक)
पालि भाषा भारतीय भाषाओं के इतिहास में अत्यंत गौरवशाली स्थान रखती है। यह न केवल बौद्ध धर्म के प्राचीन साहित्य की भाषा थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली प्रचलित लोकभाषाओं में से भी मानी जाती है।
‘पालि’ शब्द की उत्पत्ति
‘पालि’ शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसका अर्थ और मूल निम्न प्रकार दिया गया है—
| विद्वान | व्युत्पत्ति/अर्थ |
|---|---|
| आचार्य विधुशेखर | पन्ति > पत्ति > पट्टि > पल्लि > पालि |
| मैक्समुलर | पाटलिपुत्र या पाऽलि |
| भिक्षु जगदीश कश्यप | परियाय > पलियाय > पालियाय > पालि |
| भण्डारकर एवं वाकर | प्राकृत > पाकट > पाअड > पाउल > पालि |
| कोसाम्बी | पाल् > पालि |
| उदयनारायण तिवारी | पा + णिज् + लि = पालि |
इन व्युत्पत्तियों से स्पष्ट है कि पालि शब्द का आशय धीरे-धीरे “धार्मिक उपदेशों की भाषा” से “बौद्ध साहित्य की मानक भाषा” तक विस्तृत हो गया।
पालि – बुद्ध वचन की भाषा
पालि शब्द का अर्थ कई ग्रंथों में “बुद्ध वचन” बताया गया है—
“पा रक्खतीति बुद्धवचनं इति पालि।”
अर्थात् वह भाषा जिसमें बुद्ध के उपदेश संकलित हैं, पालि कहलाती है।
यही कारण है कि पालि साहित्य का मूल त्रिपिटक माना जाता है, जो बौद्ध धर्म का प्रामाणिक दार्शनिक आधार हैं।
त्रिपिटक : पालि साहित्य की आधारशिला
त्रिपिटकों की संख्या तीन है—
- सुत्त पिटक
- विनय पिटक
- अभिधम्म पिटक
(1) सुत्त पिटक
यह साधारण बातचीत के रूप में बौद्ध उपदेशों का संकलन है। इसमें पाँच निकाय हैं—
- दीर्घ निकाय
- कज्जिम (मज्झिम) निकाय
- संयुक्त निकाय
- अंगुत्तर निकाय
- खुद्दक निकाय
खुद्दक निकाय में पंद्रह प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें धम्मपद, उदान, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक आदि अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
(2) विनय पिटक
इस पिटक में बुद्ध द्वारा संघ के नियमों, आचारों और संगठनात्मक व्यवस्था का वर्णन है। इसमें पाँच ग्रंथ हैं—
- महावग्ग
- चुल्लवग्ग
- पाचित्तिय
- पाराजिक
- परिवार
(3) अभिधम्म पिटक
इसमें चित्त, चैतसिक तत्वों तथा मानस सिद्धांतों का विश्लेषण है। यह बौद्ध दर्शन का दार्शनिक भाग है। इसमें सात ग्रंथ हैं—
- धम्म संगणी
- विभंग
- धातुकथा
- पुग्गल-पंचत्ति
- कथावत्थु
- यमक
- पट्टान
पालि का भौगोलिक क्षेत्र
पालि भाषा के उद्गम स्थल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहे हैं। विभिन्न विद्वानों के मत निम्न प्रकार हैं—
| विद्वान | पालि का क्षेत्र |
|---|---|
| श्रीलंकाई बौद्ध व चाइल्डर्स | मगध |
| वेस्टरगार्ड व स्टेनकोनो | उज्जयिनी या विन्ध्य प्रदेश |
| ग्रियर्सन व राहुल | मगध |
| ओलडेनबर्ग | कलिंग |
| रीज डेविड्स | कोसल |
| चटर्जी | मध्यदेश |
| शर्मा व उदयनारायण तिवारी | मथुरा एवं मध्यदेश |
सर्वमान्य रूप से इसे मध्यदेश की लोकभाषा माना जाता है।
पालि व्याकरण और उसके प्रमुख ग्रंथ
पालि भाषा के तीन प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं—
| व्याकरण | रचयिता | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| कच्चान व्याकरण | कच्चान | 4 कप्प, 23 परिच्छेद, 675 सूत्र |
| मोग्गलान व्याकरण | मोग्गलान | 817 सूत्र, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है |
| सद्दनीति व्याकरण (1154 ई.) | भिक्षु अग्गवंश | 27 अध्याय, 1391 सूत्र |
पालि वर्ण-संरचना
पालि में कुल ध्वनियों की संख्या—
- कच्चायन के अनुसार – 41
- मोग्गलान के अनुसार – 43
स्वर
| प्रकार | स्वर |
|---|---|
| ह्रस्व | अ, इ, उ, एँ, ओं |
| दीर्घ | आ, ई, ऊ, ए, ओ |
व्यंजन-वर्ग
- क-वर्ग : क, ख, ग, घ, ङ
- च-वर्ग : च, छ, ज, झ, ञ
- ट-वर्ग : ट, ठ, ड, ढ, ण
- त-वर्ग : त, थ, द, ध, न
- प-वर्ग : प, फ, ब, भ, म
- अन्य : य, र, ल, व, स, ह, ळ, अं
पालि भाषा की भाषिक विशेषताएँ
- अनुस्वार (अं) पालि में स्वतंत्र ध्वनि है और इसे निग्गहीत कहा गया है।
- पालि में त्रि-लिंग, द्वि-वचन के स्थान पर केवल दो वचन — एकवचन और बहुवचन प्रयुक्त होते हैं।
- इसमें द्विवचन का अभाव है।
- पालि हलन्त रहित भाषा मानी जाती है।
- इसमें छह कारक, आठ लकार और आठ गणों का प्रयोग मिलता है।
- वैदिक की भांति इसमें संगीतात्मक व बलात्मक दोनों प्रकार के स्वराघात मिलते हैं।
पालि साहित्य का विस्तार और प्रभाव
पालि भाषा ने भारतीय भाषाओं के साथ-साथ एशिया के कई देशों की संस्कृति को भी प्रभावित किया। यह भाषा भारत से निकलकर—
- श्रीलंका
- बर्मा (म्यांमार)
- चीन
- तिब्बत
- थाईलैंड
- जापान
तक धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।
विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों में— अट्ठकथा साहित्य, मिलिन्दपन्हो, दीपवंश, महावंश— विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पालि का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह भाषा न केवल बुद्ध के उपदेशों की वाहक रही, बल्कि भारतीय भाषाओं के मानकीकरण और सरलीकरण की आधारशिला भी बनी। संस्कृत की जटिल संरचना को छोड़कर लोकभाषा के रूप में विकसित हुई पालि ने आगे चलकर प्राकृत और फिर अपभ्रंश के रूप में भारतीय भाषिक इतिहास को नया स्वरूप प्रदान किया।
2. प्राकृत भाषा (1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक)
(द्वितीय प्राकृत / मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा)
भारत की भाषिक परंपरा में प्राकृत भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा भी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं के इतिहास में संस्कृत और अपभ्रंश के मध्य जो भाषा विकसित होकर साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हुई, वही प्राकृत कहलाती है। यह न केवल प्राचीन भारतीय समाज की जनभाषा थी, बल्कि साहित्य, नाट्य और धार्मिक परंपराओं के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है।
प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति
‘प्राकृत’ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के दो मत मिलते हैं—
1. प्राकृत: प्राचीनतम जनभाषा का रूप
कुछ भाषाविदों का मत है कि प्राकृत मानव की सहज अभिव्यक्ति तथा मूल वाक-रूप है। इस दृष्टि से ‘प्राकृत’ शब्द ‘प्राक् + कृत’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है — पूर्वकाल में निर्मित।
नामि-साधु ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्राकृत वह भाषा है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई, जिसमें व्याकरणिक बंधन नहीं थे तथा जिसका प्रयोग सामान्य जन समुदाय द्वारा किया जाता था। इस आधार पर प्राकृत को मानव का सहज वाक्-स्वरूप माना गया।
वाक्पतिराज ने भी इसी मत को समर्थन देते हुए लिखा है कि जैसे सभी नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं और पुनः वहीं से प्रवाहित होती हैं, वैसे ही सभी भाषाएँ प्राकृत से उत्पन्न होती हैं और अंत में उसी में मिल जाती हैं।
2. प्राकृत: संस्कृत की उपजात भाषा
दूसरी धारणा के अनुसार प्राकृत संस्कृत की विकसित जनभाषा है। हेमचन्द्र, लक्ष्मीधर, वासुदेव तथा सिंह देवमणि जैसे विद्वानों ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृत संस्कृत की विकृति अथवा सरल जन-रूप है।
अब अधिकांश भाषाविद् यही स्वीकार करते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और कालांतर में यह लोकभाषा के रूप में विकसित हो गई।
प्राकृत का साहित्यिक रूप
प्राकृत का दूसरा प्रमुख नाम साहित्यिक प्राकृत है। भरतमुनि ने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में सर्वप्रथम प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा नाट्य-परंपरा में इनके प्रयोग का उल्लेख किया।
भरतमुनि द्वारा प्राकृत का वर्गीकरण
भरतमुनि ने प्राकृत को दो श्रेणियों में विभाजित किया—
| मुख्य प्राकृत | गौण विभाषाएँ |
|---|---|
| मागधी | शाबरी |
| अवन्तिजा | आभीरी |
| प्राच्या | चाण्डाली |
| सूरसेनी / शौरसेनी | सचरी |
| अर्धमागधी | द्राविड़ी |
| बाहलीक | उद्रजा |
| दाक्षिणात्य (महाराष्ट्री) | वनेचरी |
प्राकृत व्याकरण परंपरा
प्राकृत व्याकरण की परंपरा में वररुचि (7वीं शताब्दी) का नाम सर्वप्रथम आता है। उनकी कृति प्राकृत-प्रकाश (12 परिच्छेद) में उन्होंने प्राकृत को चार मुख्य उपभाषाओं में विभाजित किया—
- महाराष्ट्री
- पैशाची
- मागधी
- शौरसेनी
बाद में हेमचन्द्र ने इस सूची में तीन और नाम जोड़े—
- आर्षी (अर्धमागधी)
- चूलिका पैशाची
- अपभ्रंश
हेमचन्द्र को प्राकृत व्याकरण का पाणिनी कहा जाता है।
प्रमुख प्राकृत उपभाषाएँ
1. महाराष्ट्री प्राकृत
- इसका उद्गम महाराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है।
- डॉ. हार्नले के अनुसार इसका अर्थ है – महान राष्ट्र की भाषा।
- जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लाक ने इसे मराठी भाषा का आधार माना है।
- आचार्य दण्डी के अनुसार महाराष्ट्री सर्वश्रेष्ठ प्राकृत थी।
- प्रमुख रचनाएँ—
- राजा हाल की गाथा-सप्तशती
- प्रवरसेन की रावण-वहो
- वाक्पति की गौडवध
- वज्जालग्ग और कुमारपालचरित
2. शौरसेनी प्राकृत
- यह मथुरा और मध्य देश की भाषा थी।
- नाटकों में गद्य के रूप में इसका प्रयोग होता था।
- वररुचि ने इसे प्राकृत की मूल भाषा माना।
- कई विद्वानों के अनुसार यह संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों की आधारभूत भाषा है।
3. पैशाची प्राकृत
- इसे भूतभाषा, ग्राम्य भाषा या पैशाचिकी भी कहा जाता है।
- ग्रियर्सन के अनुसार यह अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिम पंजाब की प्रादेशिक भाषा थी।
- यह मुख्यतः राक्षसों, पिशाचों और दूसरों पात्रों के संवादों में प्रयुक्त होती थी।
- मार्कण्डेय ने इसे तीन रूपों में विभाजित किया—
- कैकयी पैशाची
- शौरसेनी पैशाची
- पाचाल पैशाची
4. मागधी प्राकृत
- यह मगध क्षेत्र की प्रमुख जनभाषा थी।
- इसके कई उपरूप प्राप्त होते हैं — शाकारी, चाण्डाली तथा शाबरी।
- अश्वघोष के नाटकों में इसका प्रारंभिक स्वरूप मिलता है।
- भरतमुनि के अनुसार यह नौकरों और सामान्य जन की बोली थी।
5. अर्धमागधी प्राकृत
- यह मगध और मध्यदेश के मध्य स्थित क्षेत्र की भाषा थी।
- जैन साहित्य में इसी का प्रयोग प्रमुखता से हुआ।
- भगवान महावीर का संपूर्ण उपदेश इसी भाषा में उपलब्ध है।
- जैन आचार्यों ने इसे ऋषिभाषा और आदिभाषा तक कहा है।
प्राकृत भाषा भारतीय भाषिक परंपरा का वह मध्यवर्ती स्वरूप है जिसने संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच पुल का कार्य किया। साहित्य, नाटक, धर्म तथा संस्कृति की अभिव्यक्ति में इस भाषा का योगदान अमूल्य है। समय के साथ प्राकृत उपभाषाएँ विकसित होती गईं और अंततः उनसे अपभ्रंश तथा आगे चलकर हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली और अन्य नई भारतीय भाषाएँ विकसित हुईं।
अतः कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाओं की जड़ में प्राकृत वह स्रोत है जिसने भारतीय अभिव्यक्ति को लोकजीवन से जोड़कर साहित्य और भाषा को समृद्ध बनाया।
अपभ्रंश भाषा (500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक)
भारतीय आर्यभाषाओं के विकासक्रम में अपभ्रंश भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भाषा प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के मध्य विकसित हुई, इसलिए इसे भाषाविज्ञानियों ने एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश मात्र एक भाषिक अवस्था नहीं, बल्कि एक साहित्यिक धारा भी थी जिसने मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और काव्य परंपराओं को नई दिशा दी।
अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति और प्रारंभिक उल्लेख
‘अपभ्रंश’ शब्द परंपरागत रूप से संस्कृत के उन रूपों को दर्शाता है जो शुद्ध व्याकरणिक नियमों से विचलित हो चुके थे। भर्तृहरि ने ‘वाक्यपदीय’ में लिखा है कि वे शब्द जो शास्त्रीय संस्कृत से हटकर व्यवहार में आते हैं, उन्हें अपभ्रंश कहा जा सकता है।
“शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते।
तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्॥”
भाषाविद् व्याडि ने सर्वप्रथम इस शब्द का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया था, यद्यपि उनके ग्रंथ लक्षश्लोकात्मक-संग्रह की प्रति उपलब्ध नहीं है।
पतंजलि के ‘महाभाष्य’ में भी ‘अपभ्रंश’ शब्द का प्रयोग मिलता है, जहाँ इसे अशुद्ध या अपशब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है—जो इस तथ्य का प्रमाण है कि अपभ्रंश रूप उस समय प्रचलित हो चुका था।
अपभ्रंश का साहित्यिक प्रयोग और मान्यता
नाट्य परंपरा में भरतमुनि अपभ्रंश का उल्लेख विभ्रष्ट भाषा के रूप में करते हैं। आगे चलकर चण्ड ने 6वीं शताब्दी में पहली बार अपभ्रंश को एक स्वतंत्र भाषा मानते हुए इसके व्याकरणिक स्वरूप की पहचान की।
राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख (वि.सं. 650 के पूर्व) में अपभ्रंश का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहाँ उनके पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि बताया गया है। यह प्रमाण इस भाषा की साहित्यिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
महाकवि भामह तथा आचार्य दण्डी दोनों ने अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के समान ही औपचारिक साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। दण्डी ने तो समूचे वाङ्मय को चार स्तरों में बाँटकर—संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र—अपभ्रंश को सम्मानजनक स्थान दिया।
अपभ्रंश के विभिन्न नाम और रूप
इतिहास में अपभ्रंश को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया, जैसे—
- अवहट्ट
- अवहंस
- पटमंजरी
- आभीर
- औहट
- अवहट
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे ण–ण भाषा कहा है, जो इसके विशिष्ट ध्वन्यात्मक स्वभाव की ओर संकेत करता है।
अपभ्रंश का क्षेत्रीय वर्गीकरण
विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश की विविध बोलियों एवं भेदों का उल्लेख किया है:
| विद्वान | वर्गीकरण |
|---|---|
| नमि साधु | उपनागर, आभीर, ग्राम्य |
| मार्कण्डेय | नागर, उपनागर, व्राचड |
| याकोबी | पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी |
| तागरे | पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी |
| नामवर सिंह | पूर्वी एवं पश्चिमी |
भाषाविज्ञानी डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं, बल्कि भाषा-स्थिति है। उनके अनुसार प्रत्येक प्राकृत भाषा का अपना अपभ्रंश स्वरूप रहा होगा — उदाहरणार्थ:
- मागधी प्राकृत → मागधी अपभ्रंश
- अर्धमागधी प्राकृत → अर्धमागधी अपभ्रंश
- शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश
- महाराष्ट्री प्राकृत → महाराष्ट्री अपभ्रंश
अपभ्रंश की ध्वनि-प्रणाली
डॉ. उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है:
स्वर (10)
- ह्रस्व: अ, इ, उ, एँ, ओँ
- दीर्घ: आ, ई, ऊ, ए, ओ
व्यंजन (30)
- कण्ठ्य: क, ख, ग, घ
- तालव्य: च, छ, ज, झ
- मूर्धन्य: ट, ठ, ड, ढ, ण
- दन्त्य: त, थ, द, ध, न
- ओष्ट्य: प, फ, ब, भ, म
- अन्तस्थ: य, र, ल, व
- ऊष्म: स, ह
अपभ्रंश की भाषिक विशेषताएँ
अपभ्रंश भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:
- इसे उकार-प्रधान भाषा कहा गया है, क्योंकि शब्दावली में ‘उ’ ध्वनि की प्रचुरता मिलती है।
- यह वियोगात्मक भाषा थी—अर्थात् विभक्तियों की बजाय स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होता था।
- अपभ्रंश में केवल दो वचन (एकवचन और बहुवचन) तथा दो लिंग (पुल्लिंग और स्त्रीलिंग) पाए जाते हैं।
अवहट्ट : अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के मध्य सेतु
समय के साथ अपभ्रंश एक नए रूप में विकसित हुआ जिसे अवहट्ट कहा जाता है। यह आधुनिक उत्तर भारतीय आर्यभाषाओं की जननी मानी जाती है।
‘अवहट्ट’ शब्द का प्रथम उल्लेख ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्णरत्नाकर में मिलता है।
अपभ्रंश भारतीय भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण है। इसने न केवल हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी आदि भाषाओं के गठन में मूलभूत योगदान दिया, बल्कि साहित्यिक परंपरा को गतिशीलता और लोकतांत्रिक स्वर प्रदान किया।
संस्कृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं की यात्रा में अपभ्रंश वह निर्णायक कड़ी है जिसने भाषा को शास्त्रीय बंधनों से मुक्त कर जनजीवन से जोड़ा।
निष्कर्ष
भारतीय आर्यभाषाओं के विकासक्रम में पालि, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पालि वह भाषा थी जिसने संस्कृत की जटिल विद्वतापूर्ण परंपरा से हटकर लोकजीवन से संवाद स्थापित किया और बुद्ध के उपदेशों को सरल रूप में जन-जन तक पहुँचाया। इसी लोकाभिमुख चेतना ने आगे चलकर प्राकृत को जन्म दिया, जिसने भारतीय साहित्य, संस्कृति और धर्म के प्रसार में मध्यवर्ती स्वरूप के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राकृत की विविध उपशाखाओं ने न केवल भाषा की संरचनात्मक सरलता को आगे बढ़ाया, बल्कि अभिव्यक्ति को अधिक मानवीय और व्यवहारिक रूप प्रदान किया।
समय के साथ जब प्राकृत रूप और अधिक परिवर्तित हुआ, तब उससे अपभ्रंश का जन्म हुआ, जिसने संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य अंतिम संक्रमण-कालीन भाषा के रूप में कार्य किया। अपभ्रंश ने साहित्य और भाषा को राजसी तथा शास्त्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर सामाजिक वर्गों तक पहुँचाया। यही वह भाषा थी जिसने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को जन्म देने में निर्णायक भूमिका निभाई।
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक यात्रा केवल भाषाई परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक विकास की निरंतर प्रक्रिया है। पालि ने संवाद की सरलता दी, प्राकृत ने साहित्यिक रूप को आकार दिया और अपभ्रंश ने आधुनिक भाषाओं की नींव रखकर भारतीय भाषिक विरासत को व्यापक, जीवंत और लोकाभिमुख बनाया।
इन्हें भी देखें –
- प्राचीन भारतीय आर्यभाषा | 1500 ई.पू. – 500 ई.पू. | उत्पत्ति, विकास और भाषिक संरचना
- आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : परिचय, विकास, स्वरूप, विकास क्रम और वर्गीकरण
- भारतीय आर्य भाषा परिवार | भारोपीय (भारत-यूरोपीय) भाषा परिवार | इंडो-आर्यन भाषा
- भारतीय आर्य भाषा : उत्पत्ति, स्वरूप और सांस्कृतिक–भाषाई विकास
- अपभ्रंश भाषा (तृतीय प्राकृत): इतिहास, विशेषताएँ, वर्गीकरण और काल निर्धारण
- प्राकृत भाषा (द्वितीय प्राकृत): उत्पत्ति, विकास, वर्गीकरण और साहित्यिक स्वरूप
- पालि भाषा (प्रथम प्राकृत): उद्भव, विकास, साहित्य और व्याकरणिक परंपरा
- नेपाली भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, दिवस और साहित्य
- भोजपुरी भाषा : इतिहास, विकास, लिपि, क्षेत्र, साहित्य और विशेषताएँ
- कौरवी बोली और नगरी (नागरी) बोली : उद्भव, क्षेत्र, विशेषताएँ और आधुनिक हिन्दी पर प्रभाव
- वैदिक संस्कृत : इतिहास, उत्पत्ति, विकास, व्याकरण और वैदिक साहित्य
- हिंदी भाषा : स्वरूप, इतिहास, संवैधानिक स्थिति और वैश्विक महत्व
- राष्ट्रभाषा : स्वरूप, अवधारणा, परिभाषा और महत्व