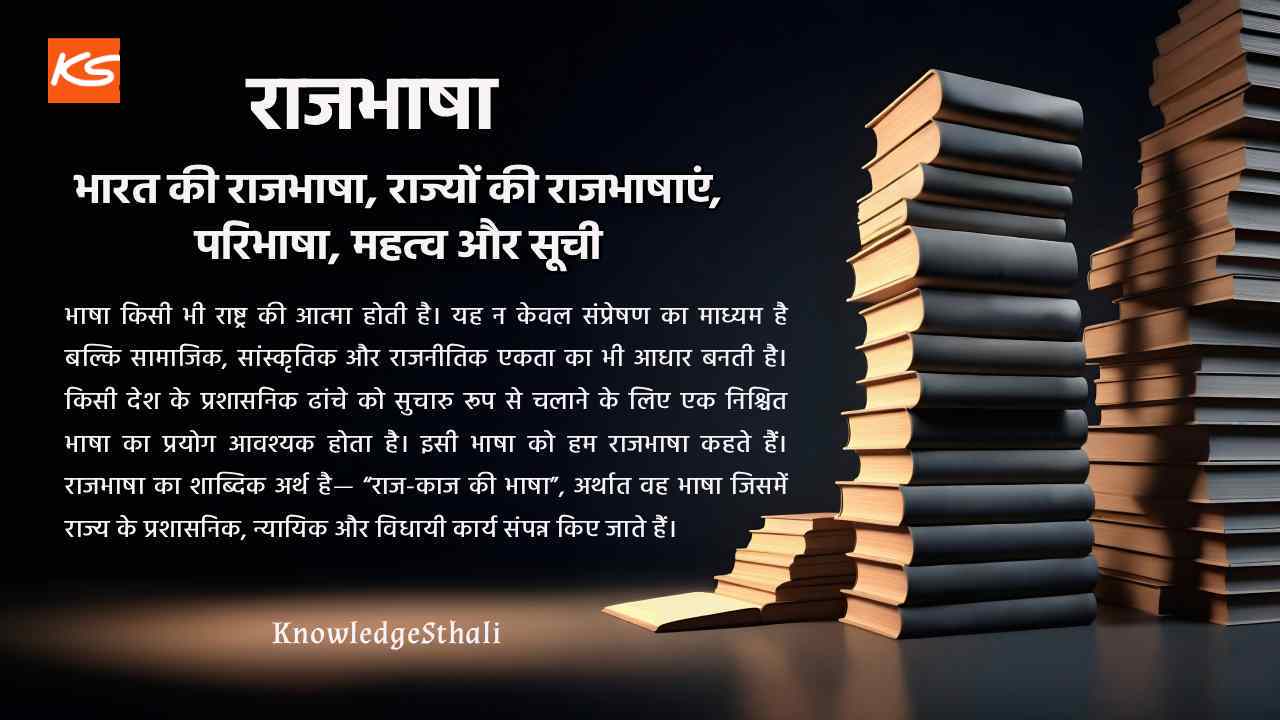भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का भी आधार बनती है। किसी देश के प्रशासनिक ढांचे को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक निश्चित भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। इसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है— “राज-काज की भाषा”, अर्थात वह भाषा जिसमें राज्य के प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी कार्य संपन्न किए जाते हैं।
भारतीय संविधान में “राजभाषा” एक संवैधानिक शब्द है, जबकि “राष्ट्रभाषा” ऐसा कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त शब्द नहीं है। यही कारण है कि हिंदी को संविधान द्वारा “राजभाषा” तो घोषित किया गया, किंतु “राष्ट्रभाषा” के रूप में नहीं। इस लेख में हम भारत की राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान, राज्यों की स्थिति, अंग्रेज़ी और हिंदी की भूमिका तथा उससे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
राजभाषा किसे कहते हैं?
राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसे किसी देश अथवा राज्य द्वारा अपने संविधान या कानून में सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कार्यों, न्यायिक प्रक्रिया और शासकीय संचार के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है।
यह भाषा शासन और प्रशासन की भाषा होती है, जिससे आदेश, अधिसूचनाएँ, सरकारी दस्तावेज़, संसद/विधानसभा की कार्यवाही और विभिन्न शासकीय विभागों का संचार किया जाता है।
👉 संक्षेप में —
- राजभाषा = सरकार की आधिकारिक भाषा
- राजभाषा वह भाषा है, जो सरकार के कामकाज और प्रशासन की आधिकारिक भाषा होती है।
- यह हमेशा राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के समान नहीं होती, क्योंकि कई देशों में प्रशासन के लिए एक भाषा तय की जाती है जबकि जनता अनेक भाषाएँ बोलती है।
भारत की राजभाषा
भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही अंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3… ) का प्रयोग निर्धारित किया गया है।
संविधान सभा में गहन विचार-विमर्श के बाद हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यद्यपि संविधान के प्रारंभ में यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों (1950–1965) तक प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए सहायक राजभाषा के रूप में किया जाएगा। परंतु बाद में हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने में विभिन्न चुनौतियों के कारण अंग्रेज़ी को भी सहायक राजभाषा के रूप में जारी रखा गया।
इस प्रकार,
- भारत की राजभाषा = हिन्दी (देवनागरी लिपि)
- सहायक राजभाषा = अंग्रेज़ी
- संविधानिक आधार = अनुच्छेद 343 से 351
👉 सरल शब्दों में कहा जाए तो हिन्दी भारत की राजभाषा है, किंतु अंग्रेज़ी भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में सहायक राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।
राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर
बहुत बार आमजन के बीच “राजभाषा” और “राष्ट्रभाषा” को समानार्थक मान लिया जाता है, जबकि दोनों की अवधारणाएँ अलग-अलग हैं।
- राजभाषा: प्रशासनिक और शासकीय कार्यों की भाषा। यह संविधान और कानून द्वारा निर्धारित की जाती है।
- राष्ट्रभाषा: किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। यह स्वाभाविक रूप से जनमानस से जुड़ती है।
भारतीय संविधान में “राष्ट्रभाषा” शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी (देवनागरी लिपि) है तथा अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में राजभाषा की यात्रा काफी लंबी और जटिल रही है।
- मुगल काल
मुग़लों के शासनकाल में फारसी राजभाषा थी। प्रशासनिक आदेश, न्यायिक फैसले और राजकीय पत्राचार फारसी में ही होता था। - अकबर से मैकाले तक
अकबर से लेकर 19वीं सदी तक फारसी का ही वर्चस्व रहा। परंतु अंग्रेज़ी सत्ता के सुदृढ़ होने के साथ ही धीरे-धीरे अंग्रेजी और उर्दू का प्रयोग बढ़ने लगा। - ब्रिटिश काल
- 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी शिक्षा नीति लागू की, जिससे अंग्रेज़ी प्रशासन और न्यायालय की मुख्य भाषा बन गई।
- 1900 में मैकडॉनेल ने उत्तर-पश्चिमी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की अदालतों में देवनागरी लिपि में हिंदी/हिंदुस्तानी के उपयोग को “अनुमेय” कर दिया।
- स्वतंत्रता से पूर्व
स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेज़ी प्रशासन की मुख्य भाषा रही। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी— इन तीन भाषाओं का प्रयोग आधिकारिक कार्यों में किया जाता रहा। - स्वतंत्रता के बाद
1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था— भारत की राजभाषा कौन होगी? बहस के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया।
संविधान और राजभाषा संबंधी प्रावधान
भारतीय संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है—
- अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय (हिन्दी-अरबी अंक) होगा।
- अनुच्छेद 344 – राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति का गठन।
- अनुच्छेद 345 – राज्य अपनी राजभाषा का निर्णय स्वयं कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 346 – राज्यों और केंद्र या दो राज्यों के बीच संचार की भाषा।
- अनुच्छेद 347 – यदि किसी राज्य की जनसंख्या का कोई भाग किसी अन्य भाषा की मांग करे, तो राष्ट्रपति विशेष उपबंध कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 348 – उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी या हिंदी का प्रयोग।
- अनुच्छेद 349 – भाषा संबंधी विधियां बनाने की विशेष प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 350 – नागरिकों को अपनी भाषा में अभ्यावेदन का अधिकार।
- अनुच्छेद 350 (क) – प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।
- अनुच्छेद 350 (ख) – भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी।
- अनुच्छेद 351 – हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन के लिए निर्देश।
हिंदी को राजभाषा बनाने की प्रक्रिया
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने बहस के उपरांत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। इसके साथ ही अंग्रेजी को एक निश्चित अवधि तक सह-राजभाषा के रूप में बनाए रखने का प्रावधान किया गया।
- संविधान लागू होने के समय प्रावधान था कि अंग्रेजी का प्रयोग अधिकतम 15 वर्षों तक (1965 तक) किया जाएगा, उसके बाद केवल हिंदी प्रयोग में लाई जाएगी।
- लेकिन हिंदी को लेकर दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों में व्यापक विरोध हुआ। परिणामस्वरूप 1963 का राजभाषा अधिनियम और बाद में 1976 के संशोधन के द्वारा अंग्रेजी को भी अनिश्चितकाल तक हिंदी के साथ बनाए रखा गया।
इसी कारण आज भी केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है।
हिंदी दिवस
14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक राजभाषा घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को “हिंदी दिवस” मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासन और जनजीवन में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।
संसद और विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा
- अनुच्छेद 120 – संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे।
- अनुच्छेद 210 – राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा।
इससे स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग संवैधानिक रूप से विनियमित है।
भारत की राजभाषाएँ और 8वीं अनुसूची
संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएँ सम्मिलित थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है—
- हिंदी
- कश्मीरी
- सिंधी
- पंजाबी
- बंगाली
- असमीया
- उड़िया
- गुजराती
- मराठी
- कन्नड़
- तेलुगु
- तमिल
- मलयालम
- उर्दू
- संस्कृत
- नेपाली
- मणिपुरी
- कोंकणी
- बोडो
- डोगरी
- मैथिली
- संथाली
राज्य सरकारें अपनी-अपनी भाषाओं को राजभाषा घोषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे—
- महाराष्ट्र में मराठी
- पंजाब में पंजाबी
- गुजरात में गुजराती
- तमिलनाडु में तमिल
- कर्नाटक में कन्नड़
भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजभाषाएँ
भारत भाषाई विविधता का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी प्रमुख भाषा है, जिसे वह अपनी राजभाषा घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार, राज्य विधानमंडल अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अपना सकता है। कई राज्यों में एक से अधिक भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
भारत के राज्यों की राजभाषाएँ
| राज्य | राजभाषा | राजधानी |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | तेलुगू | हैदराबाद / अमरावती |
| अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी | ईटानगर |
| असम | असमिया | दिसपुर |
| बिहार | हिंदी | पटना |
| छत्तीसगढ़ | हिंदी | रायपुर |
| गोवा | कोंकणी | पणजी |
| गुजरात | गुजराती | गांधीनगर |
| हरियाणा | हिंदी | चंडीगढ़ |
| हिमाचल प्रदेश | हिंदी | शिमला |
| झारखंड | हिंदी | रांची |
| कर्नाटक | कन्नड़ | बेंगलुरु |
| केरल | मलयालम | तिरुवनंतपुरम |
| मध्य प्रदेश | हिंदी | भोपाल |
| महाराष्ट्र | मराठी | मुंबई |
| मणिपुर | मीतिलोन (मणिपुरी) | इंफाल |
| मेघालय | अंग्रेज़ी | शिलांग |
| मिज़ोरम | मिज़ो, अंग्रेज़ी और हिंदी | आइजोल |
| नागालैंड | अंग्रेज़ी | कोहिमा |
| ओडिशा | उड़िया | भुवनेश्वर |
| पंजाब | पंजाबी | चंडीगढ़ |
| राजस्थान | हिंदी | जयपुर |
| सिक्किम | अंग्रेज़ी | गंगटोक |
| तमिलनाडु | तमिल | चेन्नई |
| तेलंगाना | तेलुगू और उर्दू | हैदराबाद |
| त्रिपुरा | बंगाली, अंग्रेज़ी और कोकबोरोक | अगरतला |
| उत्तर प्रदेश | हिंदी | लखनऊ |
| उत्तराखंड | हिंदी | देहरादून |
| पश्चिम बंगाल | बंगाली | कोलकाता |
भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की राजभाषाएँ
| केंद्र शासित प्रदेश | राजभाषा | राजधानी |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप | हिंदी और अंग्रेज़ी | पोर्ट ब्लेयर |
| चंडीगढ़ | अंग्रेज़ी | चंडीगढ़ |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | गुजराती, मराठी, कोंकणी और हिंदी | दमन |
| जम्मू और कश्मीर | कश्मीरी, डोगरी, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन), जम्मू (शीतकालीन) |
| दिल्ली | हिंदी | दिल्ली |
| लद्दाख | लद्दाखी, पुर्गी, हिंदी, अंग्रेज़ी | लेह, कारगिल |
| लक्षद्वीप | मलयालम और अंग्रेज़ी | कावारत्ती |
| पांडिचेरी | तमिल | पांडिचेरी |
भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की अपनी-अपनी राजभाषाएँ हैं, जो वहाँ के लोगों की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हैं। इस प्रकार, भारत की भाषाई विविधता उसकी एकता को और भी अधिक मजबूत करती है।
राजभाषा का महत्व
- प्रशासनिक एकता – राजभाषा प्रशासनिक ढांचे को एक सूत्र में बाँधती है।
- राजनीतिक-आर्थिक एकीकरण – राजभाषा एक साझा पहचान के रूप में कार्य करती है।
- सांस्कृतिक संवाहक – भाषा संस्कृति और परंपराओं को संजोने का कार्य करती है।
- राष्ट्रीय गौरव – हिंदी को राजभाषा बनाने से भारतीयता की पहचान मजबूत हुई है।
चुनौतियाँ
- भाषाई विविधता – भारत में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं। हिंदी को सभी पर थोपे जाने का भय कई राज्यों में असंतोष उत्पन्न करता है।
- अंग्रेजी का वर्चस्व – विज्ञान, तकनीक, उच्च शिक्षा और वैश्विक संवाद में अंग्रेजी का दबदबा आज भी कायम है।
- प्रशासनिक व्यावहारिकता – एक झटके में अंग्रेजी को हटाना संभव नहीं था, इसलिए द्विभाषिक व्यवस्था बनी हुई है।
- क्षेत्रीय राजनीति – दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भाषा को लेकर राजनीतिक आंदोलन समय-समय पर उभरते रहे हैं।
Quick Revision Table : भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान
| श्रेणी | विवरण | अनुच्छेद / अधिनियम / तिथि |
|---|---|---|
| संविधान में स्थान | राजभाषा संबंधी प्रावधान | भाग-17 (अनुच्छेद 343 से 351) |
| संघ की राजभाषा | हिंदी (देवनागरी लिपि) | अनुच्छेद 343 |
| संघ की अंक प्रणाली | अंतर्राष्ट्रीय रूप (हिन्दी-अरबी अंक) | अनुच्छेद 343(1) |
| राजभाषा आयोग और समिति | आयोग व संसदीय समिति का गठन | अनुच्छेद 344 |
| राज्य की राजभाषा | राज्य अपनी राजभाषा चुन सकते हैं | अनुच्छेद 345 |
| राज्य और संघ/दो राज्यों के बीच भाषा | पत्राचार हेतु भाषा | अनुच्छेद 346 |
| विशेष उपबंध (जनसंख्या के आधार पर) | किसी अन्य भाषा को मान्यता | अनुच्छेद 347 |
| न्यायपालिका और विधेयक की भाषा | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम आदि में भाषा | अनुच्छेद 348 |
| विशेष प्रक्रिया | भाषा संबंधी विधियां बनाने हेतु | अनुच्छेद 349 |
| अभ्यावेदन का अधिकार | अपनी भाषा में शिकायत / निवेदन | अनुच्छेद 350 |
| प्राथमिक शिक्षा | मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान | अनुच्छेद 350 (क) |
| भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी | अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हेतु | अनुच्छेद 350 (ख) |
| हिंदी का विकास | हिंदी को समृद्ध और वैज्ञानिक बनाने हेतु निदेश | अनुच्छेद 351 |
| हिंदी को राजभाषा घोषित | 14 सितम्बर 1949 | संविधान सभा का निर्णय |
| हिंदी दिवस | प्रतिवर्ष 14 सितम्बर | हिंदी को राजभाषा घोषित करने की स्मृति |
| राजभाषा अधिनियम, 1963 | हिंदी-अंग्रेजी दोनों के प्रयोग का प्रावधान | 1963 |
| संशोधन अधिनियम, 1976 | अंग्रेजी को अनिश्चितकाल तक जारी रखने की अनुमति | 1976 |
| 8वीं अनुसूची की भाषाएँ | वर्तमान में 22 भाषाएँ | संविधान की 8वीं अनुसूची |
निष्कर्ष
भारत की राजभाषा व्यवस्था एक व्यावहारिक और संवेदनशील समझौता है। हिंदी को राजभाषा बनाकर देश की स्वभाषा को सम्मान दिया गया, वहीं अंग्रेजी को सह-राजभाषा बनाकर प्रशासनिक निरंतरता और व्यावहारिकता सुनिश्चित की गई। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को आधुनिक विज्ञान, तकनीक, व्यापार और प्रशासन की भाषा बनाने के प्रयासों को और तेज़ किया जाए, ताकि यह केवल “कागज़ की राजभाषा” न रहकर व्यवहार की भी भाषा बन सके।
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि हम इन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में विकसित करें तो निश्चित ही भारत की पहचान विश्व पटल पर और भी सशक्त होगी।
✦ इस प्रकार राजभाषा केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय का आधार है।
इन्हें भी देखें –
- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार
- राष्ट्रभाषा : स्वरूप, अवधारणा, परिभाषा और महत्व
- हिंदी भाषा का अतीत और वर्तमान
- हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास
- हिंदी भाषा : स्वरूप, इतिहास, संवैधानिक स्थिति और वैश्विक महत्व
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता
- भाषा : परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएँ, शैली और उत्पत्ति
- हिन्दी साहित्य के 350+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
- भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद | Parts and Articles